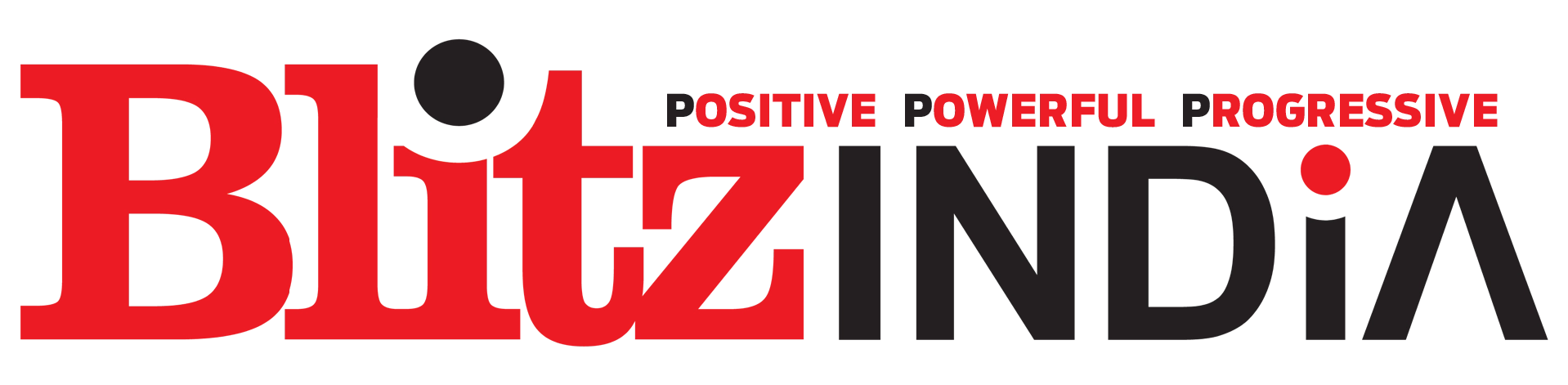ब्लिट्ज ब्यूरो
प्रयागराज। भारतीय अध्यात्म परंपरा ही नहीं, सदियों पहले से यहां आने वाले विदेशी यात्रियों ने भी अपने संस्मरण में कुंभ को दर्ज किया है।
आदि गुरु शंकराचार्य ने छठी शताब्दी ईसा पूर्व जब कुंभ को लोकप्रिय बनाना शुरू किया, तब कोई नहीं समझ सका था कि यह अनवरत चलने वाली ऐसी सनातन यात्रा प्रारंभ हो रही है, जो कालखंड में बांधी न जा सकेगी। इसके बाद सदियां बीतती गईं और कुंभ का वैभव बढ़ता गया।
सम्राट चन्द्रगुप्त मौर्य के समय (302 ईसा पूर्व) यूनानी यात्री मेगस्थनीज भारत आए थे।
उन्होंने अपनी किताब ‘इंडिका’ में गंगा किनारे लगने वाले मेले का वर्णन किया है। चीनी यात्री फाहियान (399 से 411 ई.) वाराणसी आया और गंगा से जुड़े किस्से लिखे।
सम्राट हर्षवर्धन के समय आए ह्वेनसांग ने 16 सालों तक देश के विभिन्न हिस्सों में अध्ययन किया। करीब 1400 साल पहले (644 ईस्वी) में वह सम्राट हर्षवर्धन के साथ प्रयाग कुंभ का साक्षी बना।
उन्होंने अपनी किताब ‘सी-यू-की’ में लिखा- ‘देशभर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने प्रयाग आते थे। संगम किनारे स्थित पातालपुरी मंदिर में एक सिक्क ा दान करना हजार सिक्क ों के दान के बराबर पुण्य वाला माना जाता है। प्रयाग में स्नान सभी पाप धो देता है।
अल-बिरूनी ने किताब-उल-हिन्द में देव-दानव संघर्ष का वर्णन किया। ह्वेनसांग ने प्रयागराज को मूर्तिपूजकों का महान शहर बताया और लिखा कि इस उत्सव में 5 लाख से ज्यादा लोग शामिल होते हैं। दूसरी ओर महमूद गजनवी के शासनकाल में 1030 ईस्वी के आस-पास अबू रेहान मुहम्मद इब्न अहमद अल-बिरूनी ने ‘किताब-उल-हिन्द’ लिखी। इसमें उसने वाराहमिहिर के साहित्य के आधार पर समुद्र मंथन और अमृत कुंभ को लेकर हुए देव-दानव संघर्ष का वर्णन किया है।
मुगल बादशाह अकबर 1567 में पहली बार प्रयाग पहुंचा। वह कुंभ और नागा साधुओं से भी परिचित था। अबुल फजल ने ‘अकबरनामा’ में लिखा, ‘यह स्थान प्राचीन काल से पयाग (प्रयाग) कहलाता था। बादशाह के मन में विचार था कि जहां गंगा-यमुना मिलती हैं और भारत के श्रेष्ठ लोग जिसे बहुत पवित्र समझते हैं, वहां दुर्ग बनाया जाए।’
इससे पहले सन 1398 में समरकंद से आए आक्रांता शुजा-उद-दीन तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला किया। इस दौरान उसने लूटपाट और नरसंहार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा ‘तुजुक-ए-तैमूरी’ में इसका जिक्र किया है।
गुरुचरित्र में कुम्भ की मराठी में महिमा: 14वीं शताब्दी के प्रमुख संत नृसिंह सरस्वती (1378-1459) ने मराठी में रचित अपनी पुस्तक ‘गुरुचरित्र’ में नासिक में होने वाले कुंभ मेले का विस्तार से वर्णन किया है।
त्रिस्थली में प्रयाग प्रकरणम: 16वीं सदी के मध्य में समाज गायन के प्रवर्तक नारायण भट्ट द्वारा रचित ‘त्रिस्थली सेतुः’ में वर्णित ‘अथ प्रयाग प्रकरणम’ में भी कुम्भ का विस्तृत वर्णन है।
पहला लिखित प्रमाण: ‘कुंभ मेला’ शब्द-युग्म का पहला लिखित प्रमाण मुगलकालीन गजट ‘खुलासत-उत-तवारीख’ में मिलता है। इसे औरंगजेब के शासनकाल (1695) में सुजान राय खत्री ने लिखा था। उन्होंने लिखा, कुंभ मेला हजारों वर्षों से हो रहा है।